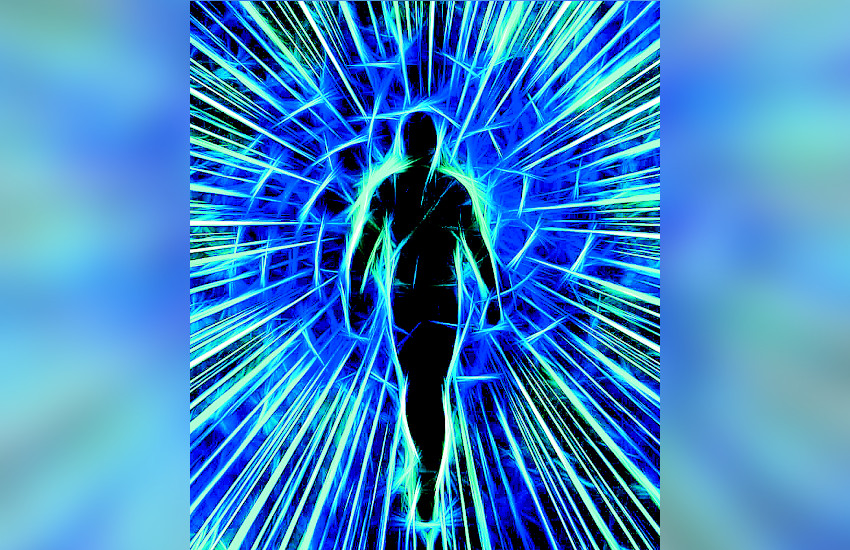ब्रह्म ज्ञान है, प्रकाश है, चेतना है। जीव है अहंकार का पर्याय, अधंकार। आवरणों में बंधा है। उन्हीं में उलझा रहता है। अत: स्वयं का बोध ही नहीं रहता। अष्टावक्र गीता (राजा जनक को सुनाई गई) इस भाव को और भी स्पष्ट करती है-
अहो निरंजन: शान्तोबोधोऽहं प्रकृते: पर:।
एतांवतमहं कालं मोहेनैव विडम्बित।। २.१ ‘मैं शान्त और दोष रहित हूं। निर्गुण हूं, किन्तु प्रकृति से आगे होकर भी माया से बंध गया हूं। मैं तो बोध हूं। मोह निद्रा में सुप्त हूू।’ गीता इसके जागरण का मार्ग खेालती है। माया और प्रकृति के स्वरूप से परिचय करवाती है।
गीता ने कर्मों को वैज्ञानिक रूप से वर्णों का आधार भी दिया। पुरुषार्थ चतुष्टय, आश्रम व्यवस्था, विद्या-अविद्या के कार्यों, प्रभावों का स्पष्ट निरूपण किया। माया और प्रकृति की व्याख्या, जीवन में उनका स्वरूप तथा कर्म फलों को प्रभावित करने की भूमिका का चित्रण करते हुए, यज्ञ-दान-तप पर भी इनका साम्राज्य बताया। ब्रह्म के विवर्त का आधार तो माया और प्रकृति ही है। यज्ञ ही सृष्टि का उपादान कारण है। यज्ञ से निर्माण क्रिया, अग्नि-सोमात्मक यज्ञ के द्वारा ही शरीरों का स्थूल भाव-प्रकृति के कार्य कहे गए हैं। प्रकृति का यह यज्ञ भी निरन्तर चलता रहता है। माया कर्म में प्रवृत्त करती जाती है, प्रकृति कर्म की दिशा तय करती जाती है। वर्ण से कर्मों की श्रेणियां भी प्रकृति के योग से ही तय होती हैं। कृष्ण सही कहते हैं कि न मैं दिखाई देता हूं (योगमाया समावृत:), न ही मैं कुछ करता हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही नष्ट न होने वाला तत्त्व हूं। यज्ञ भी हूं और कर्ता भी नहीं हूं। कृष्ण ने प्रकृति द्वारा जीव के साथ तय किए जाने वाले मार्गों की विस्तृत व्याख्या कर दी है। इसका अर्थ क्या है? यही कि यदि तुम्हारा बोध जागृत हो जाए कि तुम किस-किस कारण से, किस मार्ग से होते हुए यहां तक पहुंचे, तो अपनी योगशक्ति से पुन: उसी मार्ग से लौट सकते हो।
कर्म को जीवन में कभी नहीं छोडऩा किन्तु आसक्ति न रहना ही बुद्धियोग है। यही गीता का प्रधान लक्ष्य है। संग का अर्थ आसक्ति है। संसार आसक्ति से ही चल रहा है और यही बन्धन का कारण भी है। फल से आसक्ति हटते ही कर्म भी पूर्ण होगा, फल का बन्धन भी नहीं होगा। कर्म है तो फल भी होगा। किन्तु, आसक्ति के बिना किए गए कर्म के दो अन्य फल भी होंगे— एक, पूर्व-संचित बन्ध कटेंगे, भावी जीवन-क्रम में परिवर्तन आएगा। दो, मूल आत्म तत्त्व से जुड़ाव बढ़ेगा।
ब्रह्मï की ‘एकोऽहं बहुस्याम् प्रजायेय’ कामना ही तो कर्म का आधार है। हर व्यक्ति अपना विस्तार चाहता है। बहुस्याम्ï के लिए एक के बाद दूसरा बनना ही पड़ता है। कामना की पूर्ति में ही आनन्द है। आनन्द ही हर कामना का लक्ष्य है। यही कर्म की पूर्णता है। इसके बाद कामना समाप्त हो जाती है। ज्ञानमयी चेतना जब आनन्द भाव को छूती है, तभी ‘एकोऽहं बहुस्याम्ï’ का विचार आता है, चेतना में जागृति आती है। इसके साथ ही मन, प्राण और वाक्ï के साथ जुड़ जाता है। प्राणों की चेष्टा रूप क्रिया शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं-इस कर्म में ही मनुष्यों का मूल अधिकार है। विश्व ब्रह्माण्ड की ८४ लाख योनियों में केवल मानव ही कर्मयोनि है अन्य सभी देव, पशु, गंधर्व, वृक्षादि भोगयोनियां हैं। इसीलिए वेदव्यास लिखते हैं कि ‘न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्’ अर्थात् मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। शतपथ ब्राह्मण भी इसी का अनुमोदन करता है किन्तु वहां मानव का महत्त्व यह कहकर कई गुना अधिक कर दिया कि सृष्टि में मानव प्रजापति के सर्वाधिक निकट है-पुरुषो वै प्रजापतिर्नेदिष्ठम्। शत.ब्रा. ४.३.४.३
आत्मा मन-प्राण-वाक् की समष्टि है। सभी ८४ लाख योनियों में यह आत्मा रहता है। मन-प्राण-वाक् ही क्रमश: ज्ञान-क्रिया और अर्थ कहे जाते हैं। इनसे तीन प्रकार का आत्मा बनता है- प्रज्ञानात्मा-प्राणात्मा तथा भूतात्मा। इनमें प्रज्ञानात्मा का विकास केवल मानव में होता है। प्रज्ञानात्मक सौर प्राण इन्द्र है- यह इन्द्र इन्ध धातु से बनता है- जो प्रकाश का द्योतक है।
इस प्रकार मानव योनि में ही जीव व ईश्वर का योग संभव है। हां, तिर्यक योनियों में भी ब्रह्म प्राप्ति के उदाहरण मिलते हैं, जैसे गजेन्द्र को मोक्ष। किन्तु ऐसा प्राय: नहीं होता क्योंकि ये सभी भोगयोनियां हैं तथा प्रज्ञा प्राण का विकास इनमें नहीं होता।
कर्म अपने आप में सर्वथा शुद्ध है। मलिनता अथवा पाप-पुण्य की परिभाषा इसमें अहंकार के साथ जुड़ती है। मूल मन का, स्वयं का स्थिति-भाव व्यापक होता है, आकाश के समान होता है। त्रिगुण के कारण ही वह सीमित दिखाई पड़ता है। संकुचित होता है। और, इसी कारण कर्म का, पाप-पुण्य का जाल बनता है। यही कर्म का फल है। कर्म को बन्धन कारक मानकर त्याग नहीं सकते—चाहे प्रवृत्ति हो, या निवृत्ति। बंध भाव से छुटकारा केवल बुद्धियोग के सहारे ही मिल सकता है।
कर्म तीन प्रकार के कहे गए हैं-कर्म, अकर्म, विकर्म। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों जानने योग्य हैं क्योंकि कर्म की गति गहरी मानी गई है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण:।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति:।। गीता 4.17
तत्त्व ज्ञान के साथ मिला हुआ कर्म बन्धक नहीं होता। ज्ञान ब्रह्म का पर्याय है। यह ब्रह्म संसार में अमृत और मृत्य रूप से भासित होता है। इनको ही रस-बल, ज्ञान-कर्म भी कहा जाता है। अमृत भाग में से मृत्यु भाग को पृथक् मानना ही कर्म कहा जाता है। इस अमृत आत्मा का विरोधी कर्म विकर्म कहलाता है तथा कर्म से आसक्ति न रखते हुए कर्म करना अकर्म कहा जाता है। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हंै कि तुम अपना धर्मसिद्ध युद्ध छोड़कर जो कर्मरहित अकर्मा बनना चाहते हो, उस अकर्म में सूक्ष्मता से कर्म को देखो। राग-द्वेष-आसक्ति को छोड़कर यदि अपना धर्म मानकर युद्ध करोगे तो वह बन्धक नहीं होगा तथा अकर्म की श्रेणी में आएगा। कर्म-अकर्म अर्थात् मृत्यु और अमृत को पृथक्-पृथक् देखने वाला ही गीता में बुद्धिमान कहा गया है।
कर्म के लिए कर्म करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। अपने भीतर फल की कल्पना को ओढऩे की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हो गया, हो गया, उसका दु:ख करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म के प्रभाव गहरे हैं। हर कर्म एक संस्कार छोड़कर जाता है। यह संस्कार नया कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर नया पैदा होता है। कर्म और संस्कार का यह क्रम निरन्तर चलता रहता है। वैसे भी, आज काम करते रहने पर जोर बहुत दिया जाता है। इसके अनेक तनावों से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं। कर्म के प्रभाव को कम करने का एक ही मार्ग है, कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी फल से निवृत्त रहें। संस्कार मन में जागृत हुआ, किन्तु उसे नए कर्म रूप में नहीं बदलेंगे तो वह स्वत: ही क्षीण हो जाएगा। आगे पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, आगे का क्रम भी रुक जाएगा।