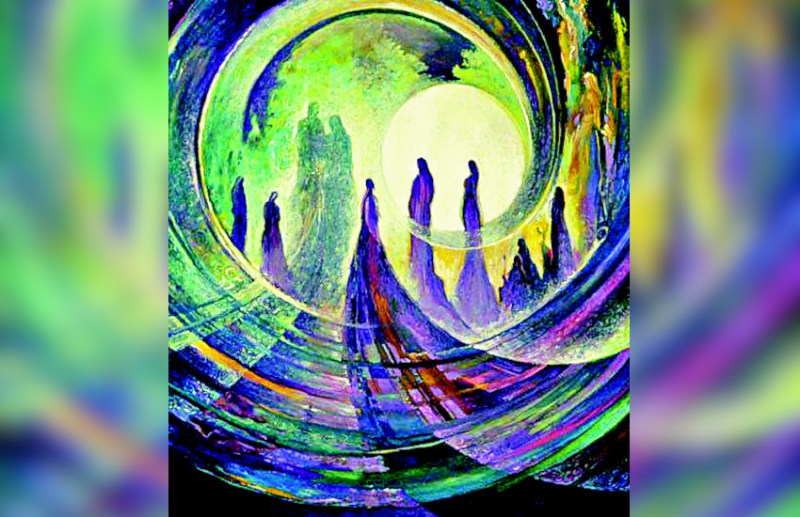
- गुलाब कोठारी
मानव जीवन कर्म प्रधान है। व्यक्तिगत कर्म व्यवहार की दृष्टि से चार आश्रम—ब्रह्मïचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास हैं और चार वर्ण—ब्राह्मïण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हैं। चार पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार भी कर्म ही हैं। कर्म ही श्रम, दान, तप और यज्ञ के रूप में स्थापित होता है जो वर्ण-व्यवस्था पर ही आधारित है। सत्व, रज और तम की शोधन रूप प्रतिष्ठा भी कर्म से ही होती है। कहने का अर्थ है कि जहां मानव जीवन है वहां कर्म है। कर्म की निश्चित व्यवस्था भी है।
कर्म दो प्रकार के होते हैं—प्राकृतिक कर्म और मनुष्यकृत कर्म। कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, आदि सब मनुष्यकृत कर्म में आते हैं। प्राकृतिक कर्म में कर्म व्यवस्था नहीं देखी जाती। आहार, निद्रा, भय, मैथुन—ये सब प्राकृतिक कर्म माने जाते हैं, जो मनुष्य और पशु में न्यूनाधिक समान रहते हैं।
जिस प्रकार हवा के प्रवाह से जल में तरंगें उठती हैं और फिर जल में ही विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार का हमारा नित्य कर्म का स्वरूप है। यदि किसी कारणवश अथवा विशेष परिस्थिति में हवा का कोई अंश पानी की पकड़ में आ जाए तो बुलबुला बन जाता है। हवा उसमें बंध जाती है। यह बुलबुला धीरे-धीरे किनारे आता है अथवा नया रूप लेने को तैयार हो जाता है, कीचड़ (पंक) बनता है। रेत, चिकनी मिट्टी आदि बना देता है। हवा और पानी दोनों का स्वरूप बदल जाता है।
जैसे वायु जल में बंधकर फेन रूप में भासित होता है वैसे ही ब्रह्मï में कर्म का पूर्णतया प्रतिभास होने से विश्व रूप बनता है। इस विश्व रूप बनने में प्रधान कारण माया कही जाती है। 'माया' शब्द का पर्याय इच्छाजनित 'कर्म' है। कर्म ही बन्धन करता है और कर्म ही बांधा जाता है। बंधित कर्म का नाम ही मृत्यु है। कर्म की ही कर्मान्तर से ग्रंथि पड़ती है। मृत्यु रूप बल रस को सीमा-भाव में लेता हुआ यदि उससे सम्बद्ध होता है तब वह ग्रंथि कहलाता है। यही कर्म का सिद्धान्त है। कर्म के इसी सिद्धान्त पर जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। कर्म के साथ ऋण जुड़ता है, उसे ऋणानुबन्ध कहते हैं।
जीवन-चक्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पूरा जीवन ही आदान-प्रदान अथवा ऋण के हिसाब-किताब की तरह चलता है। घटनाएं, दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु या नियमित जीवन-व्यवहार इसी आधार पर चलते हैं। पिछले कर्मों के अनुसार हम एक-दूसरे से व्यवहार करते हैं। कर्म के उदय के साथ ही हमारा व्यवहार बदलता है। निमित्त भी नए ऋण अथवा ऋण मोचन का एक कारण बनता है। जब ऋण चुकता हो जाता है तो विषय भी जीवन से निकल जाता है। हमारे यहां कर्म का सिद्धान्त ही जीवन का मूल आधार कहा गया है। नया जीवन इसीलिए मिलता है कि हम पुराने कर्मबन्ध या ऋणानुबन्ध समाप्त कर सकें। उनका विपाक कर सकें। इसीलिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है- न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्।
कर्म का कार्य सीमित करने का है। कर्म के अनुसार ही जीवन की सीमा भी तय होती है। जैसे ऋण पूरे हुए, जीवन समाप्त हो जाता है। जन्म के साथ ही जीवनक्रम और मृत्यु का निर्धारण भी होता है। हम इसमें फेरबदल नहीं कर पाते। हमारा प्रयास केवल यह हो सकता है कि हम पुराने ऋणों को समझकर उनका विपाक करें और नए कर्मों का जाल न बनाएं। तभी सीमित को असीम में मिला सकते हैं, अन्यथा नहीं। कर्म करो, फल से मत जोड़ो, ऋण चुकाओ और मुक्त हो जाओ।
पिछले जन्मों के कर्म व्यक्ति की आत्मा के साथ वासना-संस्कार के रूप में जुड़े रहते हैं। भीतर झांकने का जो हमारा दर्शन है वह पिछले संस्कारों को जानने तथा परिष्कृत करने के लिए है। यह हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है। यदि पूर्वकृत कर्म न होता तो यह जीवन नहीं मिलता। संसार में जो कुछ होता है, उसका कार्य-कारण भाव नियत है।
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत:।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि:।।गीता 2.16
अर्थात्-जो असत् वस्तु है उसकी सत्ता कभी नहीं हो सकती और जो सत् वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता।
यहां नियत शब्द से उन्हीं कर्मों को लेना चाहिए जिनके लिए बुद्धि की स्वत: प्रेरणा होती है। वर्णाश्रम में विहित कर्मों के प्रति बुद्धि की स्वयं प्रवृत्ति होती है। वह किसी फलाशा से मन में प्रेरणा होकर नहीं किए जाते। अत: केवल अपना धर्म समझकर अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कर्म करना बन्धक नहीं होता। ऐसे कर्म ही अकर्म अर्थात् संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध में अपने लोगों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता हूं। तब कृष्ण कहते हैं कि हम सब यदि पहले न होते तो आज भी न होते। बिना बीज और प्रयोजन के किसी की उत्पत्ति नहीं होती। यह संसार का स्थिर नियम है। पूर्वकृत कर्म ही हम सबकी उत्पत्ति का बीज हैं। साथ ही पूर्वकृत कर्मों का फलभोग ही इस जन्म का प्रयोजन है। ईश्वर द्वारा उत्पादित और प्राणियों में व्याप्त तीन प्रकार के बल-ब्रह्मबल, क्षत्रबल और विड्बल हैं। ब्रह्मबल का नाम विभूति, क्षत्रबल का ऊज्र्ज और विड्बल का श्री है। इन्हीं पर भारतीय वर्णव्यवस्था अवलम्बित है। हे अर्जुन! तुम्हारे वर्ण के अनुरूप ही तुमको कार्य करना उचित है। धर्मानुकूल युद्ध के अतिरिक्त और कोई क्षत्रिय का कल्याणकारक नहीं हो सकता। वीर क्षत्रिय अपने विशेष उद्योग से ऐसे युद्धों की योजना किया करते हैं, किन्तु तुम्हें तो यह अवसर अपने आप ही मिल गया। युद्ध, क्षत्रिय का नैतिक धर्म है। स्वधर्माचरण भी साधन दशा में ही उपयोगी होता है। वह धर्मानुकूल कर्म समत्व बुद्धि से करना चाहिए। कर्म केवल अपना कत्र्तव्य समझकर करने से बंधक नहीं होता। शास्त्रों में कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं-एक आवरक कर्म हैं जो कि बुद्धि के सात्त्विक रूप ज्ञान आदि के विरोधी हैं और दूसरे अनावरक कर्म, जो आत्मा के स्वभाव सिद्ध हैं। बुद्धि के सात्विक रूपों का आवरण नहीं करते, इन्हें ही गीता में सहज कर्म कहा गया है-सहजं कर्म कौन्तेय। यही कर्मयोग का मुख्य सिद्धान्त है कि राग-द्वेष के बिना समत्व बुद्धि से कर्म करना चाहिए। युद्ध का साक्षात् फल जय या पराजय है। यदि दोनों को समान समझ लिया जाए अर्थात् विजय में हर्ष और पराजय में दु:ख न माना जाए। यही इनकी समता कही जाती है।
सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।। गीता 2.38
सुख में विज्ञानात्मा रूप बुद्धि का विकास और दु:ख में संकोच रूप विषाद न होने दिया जाए। यही इन दोनों की समता है। केवल कर्तव्य बुद्धि से फल निरपेक्ष होकर कार्य करने से पाप और पुण्य नहीं लगते और यह कर्म आत्मा को बन्धन में नहीं डालते।
यद्यपि साधारण मनुष्य तो शरीर-यात्रा को ही आवश्यक मानते हैं। शरीर-यात्रा का निर्वाह सबके लिए ही आवश्यक है। खाना, पीना, शयन इत्यादि कर्मों के बिना यह यात्रा नहीं चल सकती। इसीलिए कर्म करना सबको आवश्यक हो जाता है। कर्मों का परित्याग कोई भी नहीं कर सकता। संन्यासमार्गी भी शरीर के आवश्यक कर्मों को नहीं छोड़ते, केवल शास्त्र निर्दिष्ट काम्य कर्मों का परित्याग करते हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम नियत कर्म करते रहो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, कर्म करना ही श्रेष्ठ है।
क्रमश:
Published on:
14 Aug 2021 07:37 am
बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग
