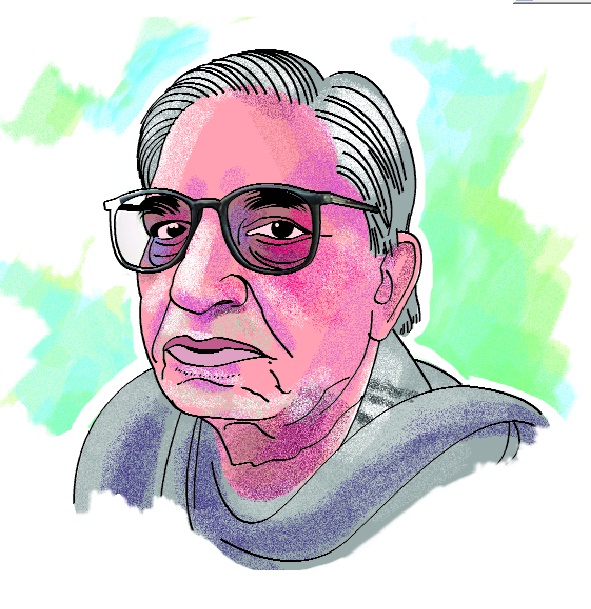
navalkishore
‘मानववाद व साहित्य’ आपकी प्रसिद्ध व चर्चित पुस्तक है। मानववाद पर आपकी क्या स्थापनाएं हैं?
मानववाद की प्रतिष्ठा यूरोपीय रेनेसां के बाद हुई और उसका लक्ष्य था मनुष्य को धर्म, ईश्वर और परलोक की अवधारणात्मक परंपरा से मुक्त करना। इस संबंध में बिना विस्तार में जाए इतना ही कह सकता हूं कि विचार की सत्ता एकदेशीय नहीं होती। वह संपूर्ण मनुष्यता की बौद्धिक विरासत में समाहित हो जाता है। धर्म और ईश्वर से जोडक़र आध्यात्मिकता को एक संकुचित अर्थ-सीमा में बांध दिया गया है। भारतीय अध्यात्म दर्शनों ने अपनी परंपराओं के मानववाद का बखान किया। यह निर्विवाद है कि मानवतावाद अर्थात प्रेम, करुणा, अहिंसा आदि के नैतिक आग्रह सभी धर्मों में विद्यमान रहे हैं। मानवतावाद से अलग मानववाद का विकास एक वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में हुआ है। आज के धार्मिक जिहादी-विग्रह मनुष्यता को किस प्रकार संतापित किए हुए हैं ये हम देख ही रहे हैं।
अच्छी आलोचना के लिए किन शर्तों को आप जरूरी मानते हैं?
आलोचना के लिए पहली प्रतिबद्धता तो साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता है। दूसरी प्रतिबद्धता मेरे विचार में किसी भी भारतीय भाषा की आलोचना में जन-प्रतिबद्धता की है। हमारा समाज न केवल एक ऐसा समाज है, जहां अनेक प्रकार के अभाव और विषमताएं हैं, बल्कि जो परंपरा और रूढिय़ों के बोझ से अत्यधिक आहत है। मैं उदाहरण सहित अपनी बात स्पष्ट करूं। कभी जन प्रतिबद्धता के आग्रह में हिंदी के जनवादियों ने साहित्यिक मूल्यों को अवमानित किया और कभी शुद्ध साहित्यवादियों ने जन-सरोकारों की सरासर उपेक्षा की। यह हमारे आधुनिक साहित्य के पाठक अच्छी तरह जानते हैं इसलिए उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आलोचक के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कैसे वह अपनी साहित्यिक प्रतिबद्धता और जन-प्रतिबद्धता के मध्य एक संतुलन बनाए रखे। आज एक ऐसे लेखक को जो साहित्य में शब्द का कमाल दिखा रहा हो उसे उस लेखक की तुलना में जो पीडि़त जन की व्यथा को संवेदनात्मक प्रभाव के साथ व्यक्त कर रहा हो, अत्यधिक महत्व देना मुझे संभव नहीं लगता है।
उत्तर आधुनिकतावाद और हिंदी आलोचना के बारे में क्या राय है?
जहां तक उत्तर आधुनिकतावाद का प्रश्न है हिंदी आलोचना में उसका शोर तो बहुत हुआ लेकिन कोई ऐसी आलोचनात्मक प्रवृति नहीं उभरी जिससे उसे उत्तर आधुनिकतावादी आलोचना कहा जा सके। मुश्किल से एक-दो आलोचकों ने इस पद्धति को अपनाया होगा लेकिन आलोचना की गति और दिशा पर कोई विशेष प्रभाव लक्षित नहीं हुआ। हां, उसके कुछ पहलुओं ने हिंदी आलोचना को प्रभावित किया। मसलन पाठ के लेखक-अभिप्रेत अर्थ की चिंता अब प्रधान नहीं रही है, अब अर्थ-बहुलता के स्वीकार के साथ पाठक को अधिक महत्व दिया जाने लगा है।
आज की बात करें तो एक हिंदी रचनाकार और आलोचक के समक्ष कौन-से संकट हैं?
सबसे पहला संकट तो प्रकाशन का है। पुस्तक-प्रकाशन की बाधा को छोड़ दें तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हिंदी के विशाल पाठक-संख्या वाले अखबारों ने साहित्य को लगभग निष्कासित कर दिया है। हां पत्रिकाएं अवश्य हैं जिनमें से अधिकतर व्यक्तिगत प्रयासों से निकल रही हैं। दूसरा संकट जो देश की राजनीति में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वह साहित्य को भी ग्रस्त कर सकता है। वह संकट है असहिष्णुता का। देश की सत्ता राजनीति में असहमति को लेकर निंदा-भाव मिलता है। हिंदी में केंद्र में आज भी जन-प्रतिबद्ध रचनाशीलता और आलोचना है। लेकिन सरकारी संस्थाओं और मीडिया आदि में इसका निंदा गान चलता रहता है। हम पाते हैं कि अमरीका जैसे घोर पूंजीवादी समाज में भी लोकतांत्रिक मूल्य इतने तिरस्कृत नहीं हैं जितने हमारे यहां। आज एक रचनाकार को जहां यह डर है कि वह किसी मिथकीय और पौराणिक पात्र को नए आलोचनात्मक ढंग से देखता है तो हो सकता है वह किसी समूह विशेष की भावना को आहत करने का अपराधी सिद्ध किया जाए।
हिंदी आलोचना की आज जो स्थिति है उसे हम गतिशीलता की श्रेणी में रखें या अवरुद्धता की?
आज आलोचना के लिए हिंदी में उपयुक्तमंच नहीं है। पत्रिकाओं में भी गंभीर सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना के लिए पृष्ठ कम ही होते हैं। पुस्तक-समीक्षा का पाठक-वर्ग कुछ बढ़ा हो सकता है किंतु आलोचना का पाठक वर्ग सीमित हो सकता है। हिंदी का समाज संख्या की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा है लेकिन साहित्य और संस्कृति सबसे अधिक उपेक्षाशील। साहित्य रचना के क्रम में जैसे बड़े रचनाकार का आविर्भाव कोई नित्य घटना नहीं है। इधर हम देख रहे हैं कि नामवरजी के बाद किसी को अभी एक बड़े आलोचक की प्रतिष्ठा नहीं मिली है। शायद इसका कारण मेरी दृष्टि-सीमा भी हो, जो अपनी पीढ़ी के बड़े उभरते आलोचक को नहीं पहचान पा रही हो।
Published on:
18 Aug 2017 07:00 pm
बड़ी खबरें
View Allखास खबर
ट्रेंडिंग
