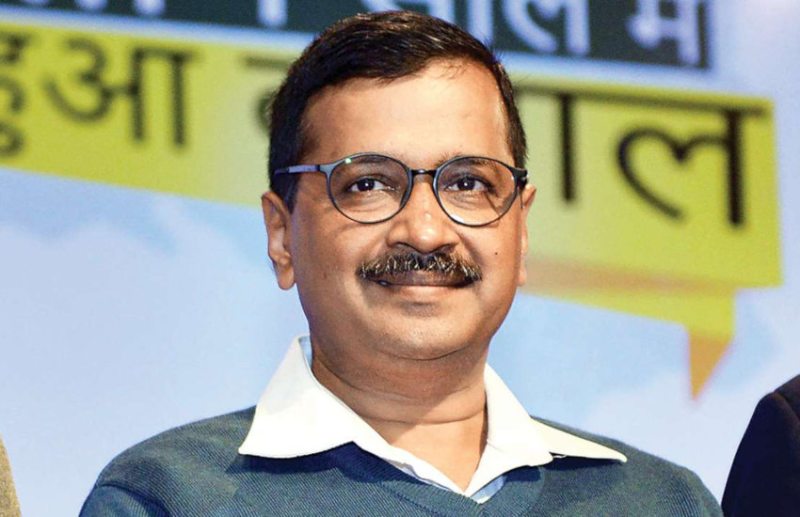
arvind kejriwal
- अभय कुमार दुबे, राजनीतिक विवेचक
भले ही एक आधी-अधूरी विधानसभा की हो, दिल्ली की राजनीति दिल्ली की ही होती है। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों द्वारा उपराज्यपाल के बैठकघर में जारी धरने और भूख हड़ताल ने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। पहला, इस आंदोलनकारी कार्रवाई से सहकारी संघवाद की सीमाओं पर रोशनी पड़ी है। यह वही सहकारी संघवाद है, जिसकी पताका बुलंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती दौर में राज्यों को भरोसे में लेने की कोशिश की थी।
दूसरा, विपक्ष की भाजपा विरोधी एकता को इस घटनाक्रम के जरिए एक ऐसा विन्यास मिलने की संभावना खुली है जो कर्नाटक चुनाव के बाद कुछ मंद हो गई थी। कर्नाटक में एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी का साथ देने की असाधारण पहलकदमी ने विपक्ष का नेतृत्व करने की कांग्रेसी दावेदारी को मजबूत कर दिया था। लेकिन दिल्ली के टकराव ने फेडरल फ्रंट की चर्चा को एक बार फिर मुखर कर दिया है। तीसरा, अब दिल्ली की स्थानीय राजनीति में कांग्रेस को अपनी रणनीति पर लाजिमी तौर पर पुन: विचार करना पड़ेगा। उसे तय करना होगा कि वह दिल्ली सरकार के अधिकारों के प्रश्न पर कब तक भाजपा के स्वर में स्वर मिलाती रहेगी।
मोदी ने जब सहकारी संघवाद का फिकरा इस्तेमाल किया था, उस समय उन्हें यह अहसास नहीं रहा होगा कि केंद्र-राज्य संबंधों का यह मसला नीति आयोग द्वारा संसाधनों के बंटवारे का सवाल तो उठाएगा ही, साथ में इन सीमाओं को लांघ कर राजनीतिक संघर्ष के मैदान में भी चला जाएगा। पिछले छह महीने से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्य अपनी हकतलफी के खिलाफ बोल रहे हैं, और बार-बार केंद्र सरकार को इस संबंध में सफाई देनी पड़ रही है।
इससे पहले कि यह प्रश्न संतोषजनक तरीके से सुलझाया जा सकता, इसके साथ ‘लोकतंत्र में जन-प्रतिनिधि की प्रभुसत्ता’ का मुद्दा जुड़ गया है। कहना न होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना तकरीबन नामुमकिन है, और कोर्ट की भाषा में कहें तो उपराज्यपाल ‘दिल्ली के बॉस’ हैं। लेकिन यह प्रकरण पूछ रहा है कि इन दोनों स्थितियों के बीच में चुने हुए प्रतिनिधि की हैसियत क्या है? क्या एक केंद्र शासित प्रदेश में उसकी हस्ती केवल नाममात्र की है? और अगर ऐसी परिस्थिति में अफसरशाही और निर्वाचित सरकार में संघर्ष होता है तो लोकतंत्र के तकाजे से किसका पक्ष लिया जाना चाहिए? पांच मुख्यमंत्रियों (पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी) द्वारा केजरीवाल और उनकी सरकार का पक्ष लिए जाने ने निर्वाचित प्रतिनिधि की हस्ती को बल दिया है। दिल्ली जैसी ही दिक्कतें पुडुचेरी के कांग्रेसी मुख्यमंत्री नारायणस्वामी को हो रही हैं, और उन्होंने यहां तक कहा है कि वे भी केजरीवाल की तर्ज पर वहां की उपराज्यपाल किरण बेदी की बैठक में धरना देने के बारे में सोचने लगे हैं।
दिल्ली और पुडुचेरी के उदाहरण बताते हैं कि संविधान के नाम पर केंद्र सरकार किस तरह चुने हुए प्रतिनिधियों को हाशिए पर धकेल सकती है। इस फेडरल फ्रंट में यदि तमिलनाडु और ओडिशा के मुख्यमंत्री भी आ जाएं (जो आसानी से आ सकते हैं) तो भाजपा सरकार के आक्रामक केंद्रवाद के खिलाफ एक क्षेत्रीय मोर्चा खुल सकता है। कई राज्यों में सत्ता से बाहर रह कर भाजपा विरोधी राजनीति कर रही पार्टियों और उनके नेताओं (जैसे अखिलेश यादव और मायावती) की हमदर्दी भी इस मोर्चे को आसानी से मिल सकती है।
यदि कांग्रेस इस मोर्चे के साथ तालमेल बैठाने में कामयाब हो जाती है तो उभरते हुए गैर भाजपावाद का रंग-रूप बदलने में देर नहीं लगेगी। ध्यान रहे, पंजाब चुनाव के बाद विपक्षी एकता के लिए दिल्ली में हुई एक बैठक में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को शामिल नहीं होने दिया था। अब कांग्रेस का रवैया वैसा ही रहा तो विपक्षी एकता के मंच पर उसे साख का नुकसान हो सकता है।
दिल्ली की स्थानीय राजनीति कुछ ऐसी है कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ भिडऩे की अनिवार्यता के बावजूद कांग्रेस लोकसभा चुनाव बिना उसके साथ गठबंधन किए नहीं जीत सकती। आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि वर्ष 2014 में आप और कांग्रेस को मिले वोट जोड़ दिए जाएं तो भाजपा दिल्ली की सातों सीटों पर बीस से पच्चीस हजार वोटों से पिछड़ जाती है। कांग्रेस के लिए 2019 का चुनाव करो या मरो का है। उसे एक-एक सीट का हिसाब-किताब लगाना है। दिल्ली में गठजोड़ करके अगर उसे तीन या चार सीटें मिल सकती हैं तो स्थानीय राजनीति के दबावों में उन्हें खोना नासमझी मानी जाएगी।
केजरीवाल ने जब उपराज्यपाल आवास में धरना शुरू किया था, तो इसे ‘एसी में आंदोलन’ कह कर मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब लग रहा है कि उनकी इस रणनीति ने, दिल्ली हाईकोर्ट की विपरीत टिप्पणी के बावजूद, राजनीतिक आंदोलन के मैदान की सीमाओं का विस्तार कर दिया है। पंजाब चुनाव में हार से ठंडे पडऩे के बाद वे एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक कल्पनाशीलता के केंद्र में आ गए हैं। उनका यह पुनरोदय विपक्ष की राजनीति के लिए भी मुफीद लग रहा है।

बड़ी खबरें
View Allओपिनियन
ट्रेंडिंग
